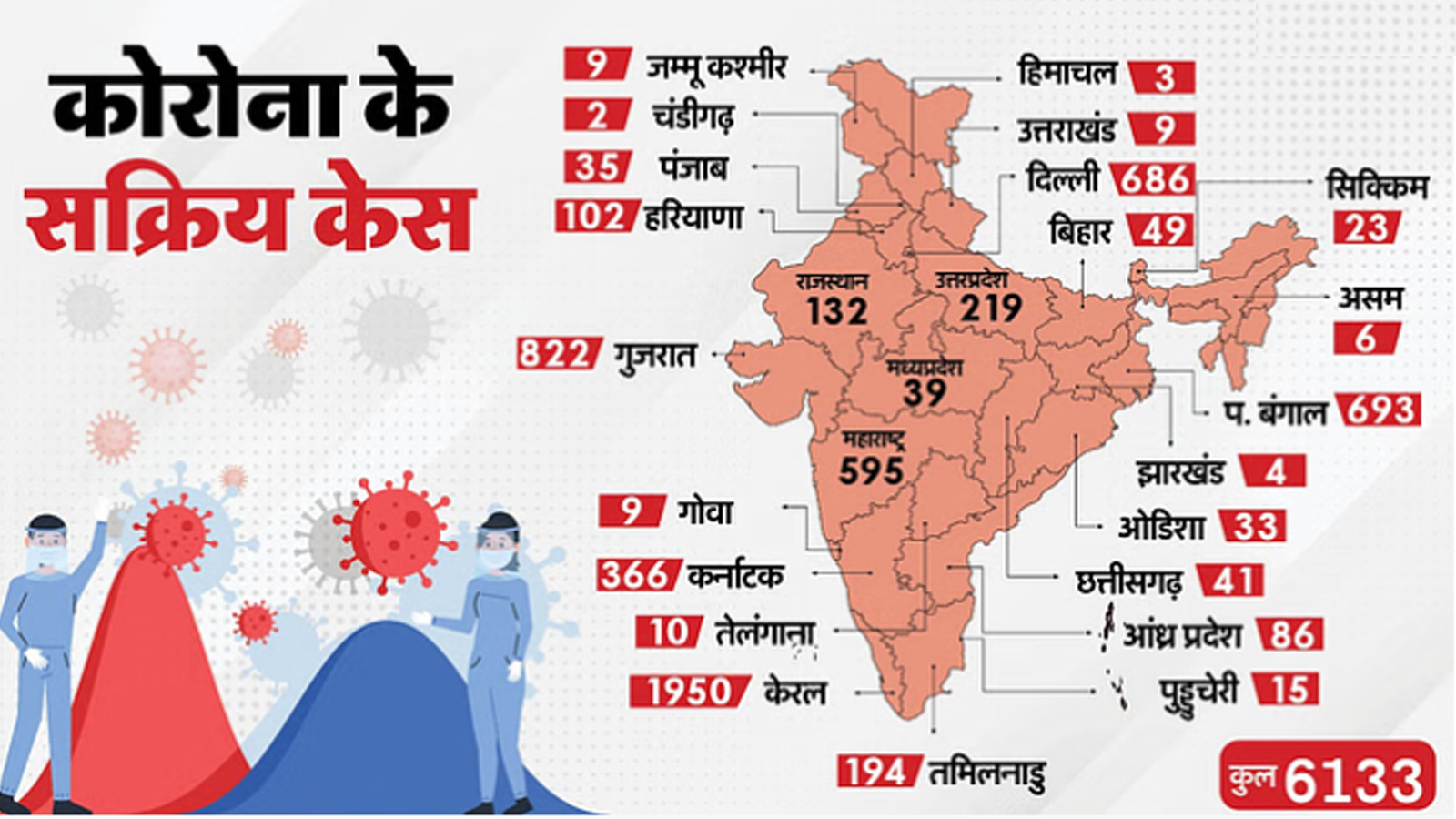सड़कों पर बढ़ते हादसों और उजड़ते सुहाग के बीच एक बार फिर राजस्व और सुरक्षा की कानूनी रस्साकशी तेज हो गई है। राजस्थान की सड़कों पर ‘मौत के सफर’ को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने जब मानवता के पक्ष में एक कठोर लकीर खींची थी, तब लगा था कि शायद अब राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों से निकलने वाला नशा राहगीरों की जान से नहीं खेलेगा। हाईकोर्ट का वह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं था, बल्कि उन हजारों परिवारों की चीख थी जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खोया है। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकारी खजाने में आने वाले इक्कीस सौ करोड़ रुपये किसी इंसान की जिंदगी की कीमत से बड़े नहीं हो सकते। यह फैसला अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को मिलने वाले ‘जीवन के अधिकार’ को सर्वोपरि रखने की एक ईमानदार कोशिश थी।
लेकिन, न्याय की इस लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक ने उन एक हजार से ज्यादा दुकानों के बाहर लटकी अनिश्चितता की तलवार को फिलहाल हटा दिया है, जो नगर निगमों और शहरी निकायों की सीमा में आती हैं। इस आदेश ने भले ही उन शराब कारोबारियों को गहरी राहत दी हो जिनके करोड़ों रुपये दांव पर लगे थे और उन सरकारी बाबुओं को सुकून दिया हो जो राजस्व के घटते आंकड़ों से परेशान थे, लेकिन सुरक्षा की उम्मीद लगाए बैठे आम आदमी के मन में एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन के लिए यह वित्तीय और व्यावहारिक प्रबंधन की चुनौती हो सकती है, मगर उन लोगों के लिए यह सीधे तौर पर जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष है जो हर रोज इन राजमार्गों पर सफर करते हैं।
अब सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जहाँ एक तरफ सरकार की वित्तीय विवशता और लाइसेंस धारकों का व्यापारिक हित है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बहते खून को रोकने की मानवीय पुकार। यह महज एक कानूनी जंग नहीं है, बल्कि इस बात का इम्तिहान भी है कि एक आधुनिक समाज के रूप में हम किसे ज्यादा महत्व देते हैं—राज्य की तिजोरी को या अपने नागरिकों की सलामती को। फिलहाल दुकानों को हटाने का आदेश टल गया है, लेकिन सड़कों पर मंडराते खतरों का समाधान अब भी भविष्य के गर्भ में छिपा है।